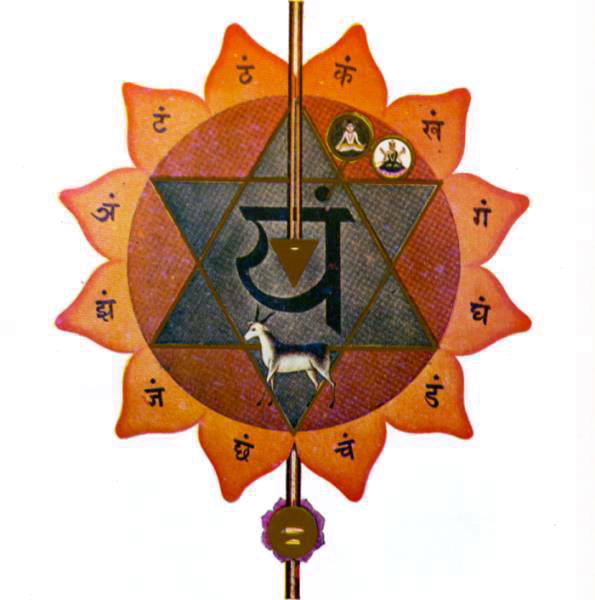वैदिक काल में ऋषियों की वाणी से जन्मा संगीत यज्ञ शालाओं, मंदिरों में ईश्वर प्राप्ति का साधन बना। मध्यकाल तक आते-आते इसने राजाश्रय प्राप्त कर दरबार की पहचान बना। ‘कलाकार द्वारा राजस्तुति का माध्यम बनने लगा कला का लक्ष्य अब मनोरंजन की सीढ़ीयाँ चढ़ने लगा जो मध्यकाल के अन्त तक आते-आते राजनैतिक आपदाओं के फलस्वरूप मंदिर में ईश्वर के निमित्त तक सीमित होने लगा। ये स्थिति आधुनिक काल के प्रारम्भिक वर्षों तक रही। काल ने करवट बदली। विष्णु द्वय के सत्प्रयासों से संगीत विद्यालयों में बच्चों की तोतली जुबानों से उच्चस्तरीय शिक्षा तक आ पहुंचा। क्योंकि यही माध्यम था जिससे संगीत पुनः जन-जन से जुड़ सके। इन विपदाओं की बदलती हुई परिस्थितियों ने संगीत पारम्परिक मनोरंजन के निमित्त सामान्य जन से दूर हो चुका था।
भारतीय संगीत की आत्मा, आध्यात्म तथा दर्शन से अनुप्रेरित है। ये हमें साकार से निराकार ब्रहृम की ओर ले जाती है। वैदिककाल में ऋृषियों की वाणी से जन्य संगीत यज्ञशालाओं, मंदिरों, दरबारों, कोठों, विद्यालयों के बच्चों की तोतली जुबानों तक पहुंचा है। ये यात्रा निश्चित रूप से काल के अनेक थपेड़ों को सहते हुए अनवरत चल रही थी। गुरु चरणों में बैठकर लिया जाने वाला ज्ञान घरानों की सीना-ब-सीना तालीम से यूट्यूब, स्काई और आनलाइन शिक्षा तक आ पहुंचा है। यद्यपि इसने वैश्वीकरण के इस दौर में भारतीय संगीत को विस्तारित किया है किन्तु कला की आत्मा का हनन भी किया है। वो भाव बोध, कला के सूक्ष्म तत्व तो गुरू चरणों में बैठकर ही प्राप्त होता है। अब भारतीय संगीत की परंपरा व प्रयोग पर दृष्टि डालें तो इसकी विशिष्टता ही इसकी प्रयोग धर्मिता है। सृजनशीलता ही इसके सौन्दर्य का आधार है। प्रत्येक कलाकार ने कला को जिस रूप में देखा, कल्पना ने कला आकाश में वैसी ही उड़ान भरी और सुन्दर व्यक्तिगत रूप में ‘रचना’ का जन्म हुआ। वही रचना जो रची गई थी बरसों बरस उसने हर मंच पर हर कलाकार के द्वारा नया रूप पाया है।
तो ये कल्पना उड़ान कब, कहाँ और कितनी हो। क्या स्वछन्द ? नहीं भारतीय कला दृष्टि सर्वथा स्वंतत्रता की पक्षपाती रही है किन्तु स्वच्छन्दता की नहीं। हमारा संगीत ठहरे पानी सा बदबूदार नहीं वरन् वो तो कल्पनारूपी नदी की नवीन लहरों से सृजित है अतः नवीन शैलियों, भावाभिव्यक्ति के सोपानों की आगमन स्वाभाविक रूप से होता ही रहा है।
हम अगर भारतीय संगीत पर विहंगम दृष्टि डालें तो गायन, वादन, नृत्य तीनों ही विधायें परंपरा और प्रयोग का आधार रही है। गायन में श्रुतिभेद 22 माने गयें किन्तु प्रयोग ने 22 श्रुतियों में असंख्य श्रुतियाँ उत्पन्न कर दी। हर स्वर भिन्न राग में अपने अलग रूप में खड़ा दिखाई देता है। यथा हम कोमल ऋषभ को भैरव, तोड़ी, भैरवी, जोगिया, बैरागी अलग-अलग रूपों में देख सकते हैं जो ‘स्वरकाकु‘ का विषय है राग रूप भी समय के अनुरूप बदलते गए बिहाग कब केवल शुद्ध मध्यम का होते-होते दोनों मध्यम का राग बन गया और संगीत जगत ने उसे यूँ ही अपना लिया पता ही न चला अगर राग रूप में प्रयोग धर्मिता न हो तो शायद ‘विवादी‘ स्वरों का कोई अस्तित्व ही न होता और नवीन रागों का निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
कला की आत्मा, सूक्ष्म तत्व व उससे जुड़े अनेक किस्से कहानियाँ तो गुरु-मुख से ही प्राप्त होता है वो ऑनलाइन शिक्षा में कहाँ।
सौन्दर्य बोध हमेशा ही काल सापेक्ष होता है। समय, काल, देश परिस्थिति के अनुकूल ही सौन्दर्य बोध बदलता रहा है अगर उदाहरण स्वरूप हम राग विस्तार को ही लें तो अतिविलम्बित लय में आलाप की दीर्घकालीन गान शैली श्रोताओं के समय, रूचि को देखते हुए को देखते हुए संकुचित हुए हैं नवीन शैलियाँ भी विकसित हुई जो घरानों का आधार बनी।
ध्रुपद जैसी पारम्परिक विधा में भी समय को देखते हुए दीर्घकालीन आलाप को संकुचित किया गया तो ‘उपज’ को बढ़ावा दिया जाने लगा जिससे श्रोताओं की सहभागिता अधिक से अधिक बनी रहे इतना ही नहीं तालों के चयन में भी लम्बे तालों की जगह कम मात्राओं के व द्रुत गति के तालों का चयन किया जाने लगा ताकि युवा पीढ़ी आकृष्ट हो।
ख्याल गायन की परंपरा इससे अछूती न रही अति विलंबित लय की गायकी के जगह थोड़ा लय बढ़ाकर गाने का चलन बन गया है आलापचारी की वेणी बन्ध शैली की जगह अब द्रुत विस्तार होने लगा है। अब एक देढ़ घण्टे के कार्यक्रम में दो राग व एक ठुमरी/भजन की परंपरा चल पड़ी है आलाप की जगह स्वर बाँट, बोल बाँट व तानों का चमत्कार शायद कलाकार व श्रोता दोनों की प्राथमिकता बन गया है यद्यपि इससे राग की आत्मा का हनन होता है किन्तु शायद कलाकारों ने समय की माँग को देखते हुए स्वीकार कर लिया है। इसी प्रकार ठुमरी दादरा जैसी उप-शास्त्रीय शैलीयाँ भी अपने आलाप की शैली को कम कर रही है।
वाद्यों के वादन में तंत्रकारी अंग की मुख्य विशेषता आलाप जोड़ कम होकर तैयारी व चमत्कार की ओर आ गए हैं। काकु भेद की दृष्टि से शब्दों के भावानुकूल एवं स्वरों एवं लयों के प्रयोग के प्रति कलाकार सजग रहते हुए गायन करता है पहले ख्याल में शब्दों को रुचिहीन समझकर स्वर के असंतुलित कर्षण से गाने की प्रथा थी। कालांतर में भाव के प्रति सजगता आई और वायस कल्चर पर ध्यान दिया जाने लगा है। नृत्य में भी तोड़े, टुकड़े, चक्करदार, सवाल-जवाब के प्रति रुझान बढ़ा है जो श्रोताओं को तो जोड़ता है किन्तु नृत्य की आत्मा व भावपक्ष की मारता है।
यद्यपि संगीत एक प्रयोग कला है किन्तु शास्त्र अपना महत्व रखता ही है खासकर शास्त्रीय संगीत तो लक्ष्य लक्षण परंपरा है अतः शास्त्र की भी अपनी एक परंपरा रही है। प्रारम्भ से ही मूलग्रन्थों के अध्ययन, मनन, चिन्तन नये सिद्धातों के प्रतिपादन की परंपरा रही है किन्तु वर्तमान में उसका स्वरूप केवल रिसर्च पेपरर्स में सिमटता जा रहा है मौलिक चिन्तन का आभाव दिखता है बहुधा कम ही मौलिक लेखक बचें हैं जो शुभ लक्षण नहीं।
भ्रान्ति थी कि ख्याल में शब्दों का कोई विशेष महत्व नहीं किन्तु कालान्तर में पं. ओंकारनाथ ठाकुर, पं. कुमार गंधर्व, विदुषि किशोरी अमोनकर जैसे विद्वान कलाकारों ने शब्द की महत्ता को समझ और स्वर, लय, आघात (टोन) के उचित प्रयोग की ओर ध्यानाकर्षित किया जिससे उबाऊ समझा जाने वाला शास्त्रीय संगीत भी रुचिकर होने लगा।
नृत्य परंपरा में भी अनेक बदलाव आए हैं कथक शैली को ही ले तो सबसे नवीन शैली और इसमें सबसे अधिक बदलाव आया है। पहले के नृत्य में जहाँ ठहराव भाव पक्ष की प्रधानता थी अगर याद करें तो कलाकरों की ‘ठाठ’ दिखाने की सम्मोहित करने वाली शैली आज भी मंत्र मुग्ध कर जाती है ग्रीवा, कटी, हस्त मुद्राओं का लयबद्ध अद्भुद संयोजन अब कहाँ, अब तो टोड़े, टुकड़े, चक्कर, परन, तिहाईयाँ के चमत्कार दिखाने की मंशा कलाकार और उसका आनन्द लेने में दर्शक को प्रभावित करती है, नृत्य की आत्मा भाव तथा ठहराव को खो गये हैं। कुछ नये प्रयोग सूफ़ी शैली जैसे अच्छे प्रयोग भी हो रहे हैं रुचिकर बनाने हेतु बैले या नृत्य नाट्य प्रयोग भी समय की मांग है जो दर्शकों को सीधा जोड़ लेती है।
आवाज का लगाव भी बदला है अगर प्रारंभिक दिनों के ग्वालियर घराने के गायकों की नाक के साथ आवाज लगाने की प्रथा थी इसी प्रकार आगरा घराने में खसखसी आवाज लगाने की प्रथा थी पटियाला घराना खुली तान दार आवाज लगाने की तालीम देता तो जयपुर घराने में आवाज का लगाव खुले गले का था किराने घराने की गोल आवाज विशिष्ट थी समय बदला वैश्वीकरण के इस दौर में घरानों के घेरे को तोड़ शिष्य विभिन्न घरानों की विशिष्टताओं से स्वयं को सृजित करने लगा है ये शुभ संकेत भी है वायस कल्चर पर ध्यान दिया जाने लगा है। अब इस प्रयोगधर्मी परंपरा में प्रयोग कहाँ तक इस पर विचार की आवश्यकता है परंपरा और प्रयोग को दो चरण मानते हुए अपनी थाती को सुरक्षित रखते हुए ही प्रयोग की ओर कदम बढ़ाना है तभी हम संगीत के शाश्वत स्वरूप का संरक्षण एवं संवर्धन कर सकेंगे